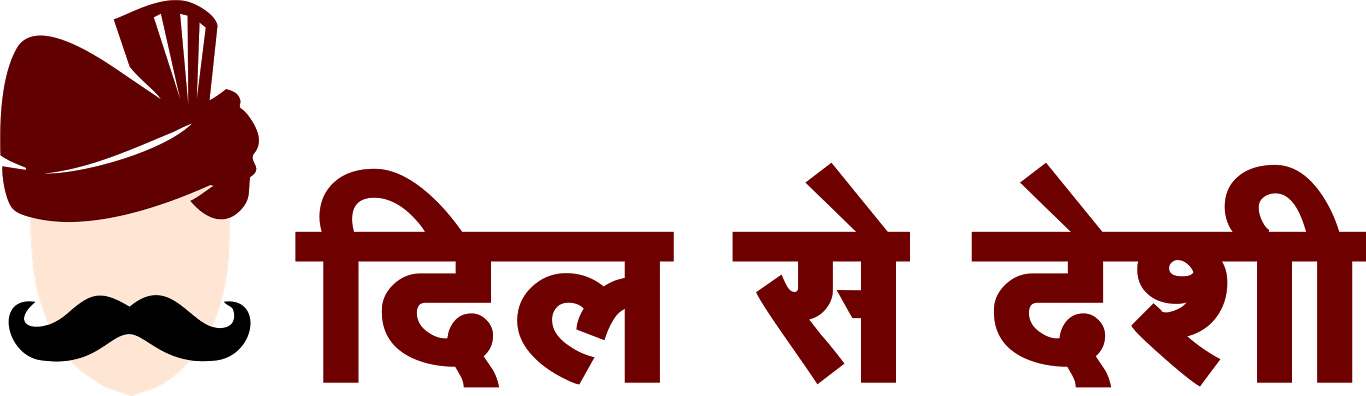संज्ञा की परिभाषा और विभिन्न भेद की जानकारी | Defination and Parts of Sangya in Hindi Vyakarana | Sagya Ki Paribhasha and Bhed
संज्ञा शब्द “सम्” और ‘ज्ञा” के योग से बना है जिसका अर्थ है “सम्यक ज्ञान” पूर्ण और सही परिचय. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, क्रिया, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है.
संज्ञा की परिभाषा (Sangya Ki Paribhasha)
“किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है”
उदाहरण
-मोहन दिल्ली में निवास करता है.
-नारियाँ स्वभाव में कोमल होती है.
–नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है.
-गाय एक पालतू पशु है.
-बुढ़ापा दु:खों का घर है.
-आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ है.
उपरोक्त काले शब्द संज्ञा शब्द है. संज्ञा शब्दों का भी इसलिए भी विशेष महत्व है. की संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती. हम जब भी कोई भी बात पूछते है, करते है तो अनायास ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते है. व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते है संज्ञा शब्द कहलाते है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति,गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते है.
संज्ञा के भेद (Sagya Ke Bhed)
संज्ञा शब्दों से प्रायः किसी व्यक्ति, जाती अथवा भाव के नाम का बोध होता है इसलिए संज्ञा के तीन प्रमुख भेद बताए गए है-
- व्यक्तिवाचक संज्ञा
- जातिवाचक संज्ञा
- भाववाचक संज्ञा
1. व्यक्तिवाचक संज्ञा (Vyaktivachak Sangya)
जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान अथवा विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है. जैसे-
व्यक्तियों के नाम- महात्मा गाँधी, सीता, गीता, रूपा, राम, लखन, रेखा, पूनम, सौरभ, अमन, सुमन, अभिषेक
प्राणियों के नाम- कपिला (गाय), सोना (हिरनी), गौरा (गाय), एरावत (हाथी)
स्थानों के नाम- दिल्ली, कानपुर, आगरा, शिमला, जापान, अमेरिका, जयपुर, सागर, मुंबई, हरियाणा
वस्तुओ के नाम- हल्दी, नमक, चीनी, कुर्सी, टेबल, किताब, पेन, रबर, कपडे.
2. जातिवाचक संज्ञा (Jativachak Sangya)
जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाती का बोध कराते है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते है. जैसे-
मनुष्य, नर, नारी, पशु, नदी, पहाड़, ग्राम, लड़का, पुस्तक, घर, नगर, पाठशाला, नदी, झरना, हाथी, कुत्ता, फल, गाय, विद्यार्थी, टीचर आदि.
( ये शब्द सम्पूर्ण जाती के परिचायक है किसी एक मनुष्य, एक नर, एक प्रान्त के नहीं)
जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है-
- द्रव्यवाचक संज्ञा
- समूहवाचक संज्ञा
अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के पांच भेद स्वीकार किये गए है. उसी आधार पर हिंदी के कुछ विद्वान् भी संज्ञा के पांच भेद मानते है. वेसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी एक प्रकार से जाति का भेद करवाती है. इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेदो के रूप में स्वीकार किया गया है.
द्रव्यवाचक संज्ञा (Dyavavachak Sangya)- किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है. जैसे-
स्टील, पीतल, तांबा, लोहा (बर्तनों के लिए)
प्लास्टिक, लकड़ी (खिलोने के लिए)
लकड़ी, लोहा (फर्नीचर के लिए)
सोना- चाँदी (आभूषण के लिए)
समूहवाचक संज्ञा (Samuhvachak Sangya)- जो संज्ञा किसी समुदाय या समूह का बोध कराते है, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते है. जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की सम्भावना होगी, जैसे-
सेना, कक्षा, भीड़, जुलूस, दरबार, दल आदि.
(इन शब्दों का प्रयोग एकवचन में ही होता है क्योकि ये एक ही जाती के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते है)
इस प्रकार हम कह सकते है की जो शब्द किसी जाती, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराते है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते है.
तुलना देखिए-
| जातिवाचक संज्ञा | बालक | स्त्री | स्थान | नदी | पुरुष | पर्वत | किताब |
| व्यक्तिवाचक संज्ञा | राम | गीता | दिल्ली | गंगा | रोहन | हिमालय | रामायण |
3. भाववाचक संज्ञा (Bhavavachak Sangya)
जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण – धर्म, दोष, शील, स्वाभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहे जाते है. जैसे-
गुण-दोष – लम्बाई, चौड़ाई, सुन्दरता, चतुराई, ऊँचाई, कुरूपता.
दशा – बचपन, बुढ़ापा, यौवन, भूख, प्यास
भाव – आशा, निराशा, क्रोध, युद्ध, शांति, मित्रता, भय, प्रेम
कार्य – सहायता, निंदा, प्रशंसा, सलाह
एक संज्ञापद का दुसरे संज्ञापद के रूप में प्रयोग
कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञापद एक दुसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते है, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवावाचक के रूप में और कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कर दिया जाता है.
1. व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग-
कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण होता है जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है. ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति- विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक शब्द बन जाते है. जैसे भीष्म पितामह का नाम दृढ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है. जैसे-
- आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है?
- भारत तो सीता- सावित्री का देश है.
- विभीषनो से बचो.
- देश में जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ.
- तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो.
(यंहा पर “हरिश्चंद्र” “सच्चाई”, “सीता- सावित्री” “पवित्रता” का, “विभीषण” “विश्वासघात” का “जयचंद” “गद्दार” का और “एकलव्य” “गुरुभक्ति” का प्रतीक है. )
2. जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग
कभी कभी कुछ जातिवाद शब्द किसी व्यक्ति- विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते है तब वे जाती का बोध न कराकर केवल एक “व्यक्ति या स्थान- विशेष” का बोध कराते है. जैसे-
- महात्मा जी ने भारत को को आजाद कराया. – महात्मा गाँधी
- स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासते समाप्त की. – सरदार पटेल
- पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे. – पंडित जवाहरलाल नेहरु
- शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे. –लाल बहादुर शास्त्री
- पुरी की पवित्रता सर्वविदित है. – जगन्नाथपुरी
3. भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग
भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एकवचन में होता है, किन्तु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते है. तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते है.जैसे-
बुराई से बुराईयाँ- हम सभी में अनेक बुराइयाँ है.
पढाई से पढाईयां- निर्धन व्यक्ति को बच्चो की पढाईयां मार देती है.
दूर से दूरियाँ- कभी कभी दूरियाँ ही अपनेपन का आभास कराती है.प्रार्थना से प्रार्थनाएँ- गरीबो की प्रार्थनाएँ व्यर्थ नहीं जाती.
ऊँचाई से ऊँचाइयाँ- ऊँचाइयाँ- ऊँचाइयाँ नापनी है तो हिमालय का भ्रमण करो.
यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द
यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना सभी प्रकार के शब्दों से हो सकती है. ये प्रायःपांच प्रकार के शब्दों से बनती है-
- जातिवाचक संज्ञाओ से
- सर्वनाम से
- विशेषणों से
- क्रियाओं से
- अव्ययो से
1. जातिवाचक संज्ञा से
| जातिवाचक शब्द | भाववाचक शब्द |
| नर | नरत्व |
| इंसान | इंसानियत |
| देव | देवत्व |
| चोर | चोरी |
| पिता | पितृत्व |
| पशु | पशुता/ पशुत्व |
| नेता | नेतृत्व |
| जवान | जवानी |
| आदमी | आदमीयत |
| अतिथि | आथित्य |
| पुरुष | पुरुषत्व |
| शिष्य | शिष्यत्व/ शिष्यता |
| गुरु | गुरुता/ गुरुत्व |
| ठाकुर | ठाकुरी/ ठकुराई |
| बालक | बालपन |
| किशोर | कैशोर्य |
| मित्र | मित्रता |
| प्रभु | प्रभुता |
| दोस्त | दोस्ती |
2. सर्वनाम से-
| सर्वनाम | भाववाचक संज्ञा |
| अहं | अहंकार |
| आप | आपा |
| अपना | अपनापन |
| निज | निजता |
| आत्म | आत्मीयता |
| पराया | परायापन |
| सर्व | सर्वस्व |
| मम | ममता |
| तेरा | तेरापन |
3. विशेषणों से-
| विशेषण | भाववाचक संज्ञा |
| उचित | औचित्य |
| आवश्यक | आवश्यकता |
| उदार | उदारता |
| अलग | अलगाव |
| कुलीन | कुलीनता |
| अच्छा | अच्छाई |
| उपयोगी | उपयोगिता |
| कुशल | कुशलता |
| कुटिल | कुटिलता |
| एक | एकता |
| आलसी | आलस्य |
| कठोर | कठोरता |
| गहरा | गहराई |
| अमर | अमरता |
| कला | कालापन |
| अगर | अगरता |
| चतुर | चतुरता |
| सुगम | सुगमता |
| वीर | वीरता |
4. क्रियाओं से-
| क्रियापद | भाववाचक संज्ञा |
| आबाद | आबादी |
| खोजना | खोज |
| जीना | जीवन |
| देखना | दर्शन |
| बनना | बनाना |
| dजलना | जलन |
| भूलना | भूल |
| बदलना | बदलाव |
| पूजना | पूजा |
| सीना | सिलाई |
| टकराना | टकराव |
| कसना | कसावट |
| चलना | चलन |
| दबाना | दाब |
| उधार | उधारी |
| नापना | नाप |
| लचकाना | लचक |
| तराशना | तराश |
| जपना | जाप |
5. अवयवो से-
| अविकारी शब्द | भाववाचक संज्ञा |
| तेज़ | तेज़ी |
| ऊपर | ऊपरी |
| निकट | निकटता |
| देर | देरी |
| जल्दी | जल्दबाजी |
| नीचे | निचाई |
| दूर | दूरी |
धन्यवाद मित्रो ! आपको हिंदी व्याकरण और संज्ञा विषय से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रुर दे.